Literature, music, dance, art and culture of Chhattisgarh.
(छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति। )
छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत
Watch Videos (Click here)
प्राचीन भारतीय मौर्यकाल, शुंग, सातवाहन कालीन एवं गुप्तकालीन संस्कृति का छत्तीसगढ़ पर प्रभाव पड़ा।
छत्तीसगढ़ के इतिहास में अनेक राजवंशों ने शासन किया जिनमें शरभपुरीय, पाण्डुवंशी, सोमवंशी, नलवंश, राजर्षितुल्य आदि राजवंशों ने अपनी विविध भूमिकाएँ प्रस्तुत की।
इन राजवंशों द्वारा अपनी पृथक-पृथक परम्पराओं और कला शैलियों को अपनी व्यक्तिगत अभिरूचि के आधार पर विकसित किया गया।
उन्होंने गुप्तयुगीन कला की शास्त्रीय परम्पराओं को अपने संस्कारों के आधार पर पल्लवित किया।
जिसके फलस्वरूप आज छत्तीसगढ़ में अद्भुत देवालयों तथा देव प्रतिमाओं के नयनाभिराम दृश्यों का अवलोकन किया जा सकता है।
इन राजवंशों के प्रसिद्ध कला केन्द्र के रूप में मल्हार, अड़भार, सिरपुर, राजिम आदि स्थल हैं।
संस्कृति
छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संबंध में अनेक विद्वानों का मत है कि यहाँ की संस्कृति मिश्रित संस्कृति की श्रेणी में आती है।
"गढ़ों का गढ़ छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक समन्वय, सामाजिक समरसता एवं सर्वधर्म समभाव का गढ़ है।
यह देश का ऐसा भू–भाग है जो उत्तर दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम सभी ओर से भारत को जोड़ता है, देश की साँस्कृतिक विरासत यहाँ के अरण्यांचल में सदियों से संरक्षित, संदर्भित एवं सुरक्षित है।"
छत्तीसगढ़ी संस्कृति की एक अपनी विशिष्ट पहचान है। अरण्यों की संस्कृति एवं प्रवासी संस्कृति के समन्वय से अद्भुत यहाँ की
एकता के विकास में छत्तीसगढ़ सहभागी रहा है।
संस्कृति की पहचान मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं के रूप में होती है। तत्पश्चात् लोगों के रहन-सहन, खान-पान और बोलचाल, वेशभूषा, बोली, भाषा आदि पर दृष्टिपात किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी स्पष्ट रूप से यहाँ की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ की धार्मिक विचारधाराओं का अवलोकन करना होगा।
छत्तीसगढ़ की धार्मिक स्थिति
छत्तीसगढ़ की धार्मिक परम्परा का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में धर्म का अस्तित्व किंवदंतियों के उस युग से आरंभ होता है, जहाँ पर इतिहासकार दृष्टिपात नहीं कर पाते।
छत्तीसगढ़ में प्राचीनकाल से ही अनेक धार्मिक मतों का प्रचलन था। वैष्णव, शाक्त, शैव, बौद्ध और जैनधर्म यहाँ के निवासियों के द्वारा अपनाए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं।
शैव धर्म: -
शैवधर्म छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्राचीन धर्म माना जाता है। किसी भी धर्म को प्रगति प्रदान करने और जन-प्रिय बनाने में तत्कालीन शासकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले कल्चुरिवंश का शैव धर्मोपासक होना इस क्षेत्र में शैव धर्म के प्रसार के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है।
नलवंशीय बस्तर के शासकों द्वारा अपने सिक्कों पर नन्दी का अंकन इस बात का द्योतक है कि वे भी शैव धर्म के अनुयायी रहे हैं। इसके उपरान्त पाण्डुवंशी शासकों ने शैवधर्म के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
वैष्णव धर्म
वाल्मीकि रामायण के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में वैष्णव धर्म का अस्तित्व रामायण काल से है। प्रमाणिक रूप से छत्तीसगढ़ में वैष्णव धर्म ईसा की पहली और दूसरी सदी में भी मौजूद था। राजिम का राजीव लोचन मन्दिर और सिरपुर का लक्ष्मण मन्दिर छत्तीसगढ़ में वैष्णव धर्म से सम्बंधित वास्तु कला के उदाहरण है।
बौद्ध धर्म
छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण पाँचवी सदी ई. का मिलता है। बस्तर के भोंगापाल नामक स्थान में मध्यप्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के दौरान एक चैत्यगृह की प्राप्ति इस अंचल में बौद्ध धर्म के अस्तित्व का प्रमाण है। इसके अन्य प्रमाण मल्हार, सिरपुर आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं।
जैन धर्म
छत्तीसगढ़ में उपलब्ध जैन प्रतिमाओं, जैन-मन्दिरों के अवशेषों, अभिलेखों आदि से यहाँ पर जैन धर्म के प्राचीनकाल से चले आ रहे प्रचलन की जानकारी मिलती है। सिरपुर, मल्हार, रतनपुर, धनपुर, अड़भार, पद्मपुर, महेशपुर, राजिम, ताला आदि स्थानों से जैन धर्म से संबंधित सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलती है जो छत्तीसगढ़ में जैन धर्म की व्यापकता के प्रमाण हैं। _आधुनिक काल में इन पुरावशेषों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की उन्नत धार्मिक सहिष्णुता के दर्शन होते हैं, साथ ही विभिन्न धर्मों की संगम स्थली होने का गौरव भी प्राप्त होता है।
छत्तीसगढ़ की सामाजिक पृष्ठभूमि वर्ण व्यवस्थाः-
छत्तीसगढ़ में प्राचीनकाल में समतियों में वर्णित वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। किन्तु उनमें कट्टरता नहीं पायी जाती थी। उदाहरणार्थ- राजपद प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं था कि इस वंश के लोग क्षत्रिय ही हों, अपितु ब्राहमण और वैश्य वर्ग के लोग भी राजा हो सकते थे। कल्चुरियों का एक सामन्त वैश्य था। उसी प्रकार शरभपुरीय राजाओं के समकालीन वाकाटक राजा ब्राह्मण थे।
चारों-वर्गों में ब्राहमणों को श्रेष्ठ माना जाता था। तत्पश्चात क्षत्रियों का स्थान था जो प्रायः राजवंशी थे। वैश्य वर्ण के लोग व्यवस्थानुसार व्यापार वाणिज्य करते थे। शूद्र वर्ण का स्थान सबसे नीचे था।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, शिल्पी, तेली, बैरागी, कुर्मी, कंवर, बनिया, गोड़, स्वर्णकार, देवार, धसिया, सतनामी, व कबीरपंथी जाति के लोग निवास करते हैं।'
रहन-सहनः-
छत्तीसगढ़ के लोगों का रहन-सहन आर्थिक एवं जातिगत आधार पर विभाजित किया जा सकता है। यहाँ के लोग प्रायः सीधा-सादा जीवन व्यतीत करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति के लोग कच्चे मकानों में रहते हैं तथा सम्पन्न लोग पक्के ईंट पत्थरों से बने मकानों में रहते हैं।
वेशभूषाः
यहाँ के पुरूषों की वेशभूषा अंगोछी, पटका या पंछा है। यह मुश्किल से घुटनों तक पहुंचती है। सम्पन्न लोग कमीज, कुर्ता, धोती पहनते हैं। महिलाएँ लुगरा साड़ी के समान पहनती है। चोली या पोलका पहनने का रिवाज पहले न के बराबर था किन्तु अब इसका प्रचलन बढ़ गया है।
आभूषण:
मुख्य रूप से पहने जाने वाले आभूषणहमेल, सुता, पुतरी, रूपया गले में पहना जाने वाला आभूषण है। पैरी, गठिया, साँटी, झाँझर, लच्छा, तोड़ा और घुघरू पैरों में पहना जाता है। पैर की अंगुलियों में चुटकी, बिछिया और अंगूठे में चुटका पहनते हैं। हाथ के आभूषण में काँच, चाँदी की चूड़ी जिसमें ऐंठी, पटा आदि आते हैं। नाक में | नथ, बेसर, लौंग, फूली धारण करते हैं। कान में झुमका वाली तरकी, बाजुओं में बहुँटा, पहुँची आदि आभूषण प्रचलित हैं।
खान-पान:
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्रायः तीन बार भोजन करते हैं। खाने में 'बासी' जो कि पानी में भीगा हुआ भात होता है। प्रमुखता से खाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में । रात का भोजन भात है। सामान्य तौर पर लोगों का भोजन दाल, चावल और सब्जी है।
विवाह:
यहाँ की अधिकाँश जातियाँ हिन्दू संस्कारों के अनुसार विवाह करती हैं। कन्या का विवाह छोटी उम्र में ही किया जाना लोग पसन्द करते हैं। यहाँ कई तरह के विवाह प्रचलित हैं, जैसे- छुट्टा-विवाह, कनियादान (कन्यादान), गुरावट, देहड़ा-विवाह तथा चढ़ विवाह। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में चूड़ी पहनाने की प्रथा भी प्रचलित है।
शिक्षा:
छत्तीसगढ़ में 1818 के पूर्व शिक्षा का प्रसार नहीं के बराबर था। उच्च जाति के लोग अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था स्वयं घर पर करते थे। शिक्षा देने का कार्य करने वाले व्यक्ति को भेंट स्वरूप अन्न, वस्त्रादि प्राप्त होता था। पाठशाला मन्दिरों में या वृक्षों के नीचे लगती थी। शिक्षा का माध्यम हिन्दी था।
मनोरंजन के साधन:
मनोरंजन के साधन में मुख्य रूप से नृत्य, संगीत, चौपड़, जुआ, मुर्गों की लड़ाई प्रचलित है। बच्चों में गुल्ली-डंडे का प्रचलन है। साधारण जनता राऊत नाचा, डण्डानाच, रासलीला-नाटक आदि से अपना मनोरंजन करते हैं।
प्रमुख पर्व:
छत्तीसगढ़ अंचल तीज-त्यौहार का अंचल है। यहाँ अनेक तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख त्यौहारों में -हरेली, नागपंचमी, रामनवमी, दीपावली, होली, भोजली, रक्षाबंधन, हलषष्ठी, हरितालिका व्रत, बहुरा-चौथ, रथ-यात्रा, भीमसेनी एकादशी, इतवारी और बुधवारी त्यौहार अगहन के बृहस्पतिवार की लक्षमी पूजा, जन्माष्टमी, पोला, नवरात्र, विजयादशमी, गोवर्धन पूजा, छेरछेरा आदि छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व हैं।
विभिन्न कलाएँ
मूर्तिकला:-
छत्तीसगढ़ की मूर्तिकला गुप्तकाल के बाद की मानी जाती हैं। इसे कला का संक्रमण युग भी कहा जाता है। संक्रमण काल की मूर्तिकला को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जिसमें प्रथम वर्ग में भित्ति स्तम्भों पर उत्कीर्ण विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियाँ हैं- जो राजिम के राजीव लोचन, खरौद के लक्ष्मणेश्वर, भोरमदेव, बालोद और देवरबीजा में स्थित हैं। द्वितीय वर्ग की मूर्तियाँ स्वतंत्र रूप में स्थित हैं। इनको मंदिरों के प्रांगण में स्थापित किया गया। इनमें सिरपुर से प्राप्त 'मन्जुश्री' व विष्णु की मूर्ति, राजिम से प्राप्त वामन और त्रिविक्रम मूर्तियाँ प्रमुख हैं। इन मूर्तियों में कला की विकसित परम्परा दिखती है।
छत्तीसगढ़ के स्थापत्य और मूर्ति शिल्प में यहाँ के लोकजीवन में प्रचलित वेशभूषा, नृत्य, संगीत, आखेट आदि के दर्शन होते हैं। यहाँ के विभिन्न स्थापत्य केन्द्रों में क्षेत्रीय लोककला और सामान्य जन का अंकन मिलता
चित्रकला:-
छत्तीसगढ़ में लोक चित्रकला की एक समृद्ध परम्परा प्रचलित है। यहाँ अनेक प्रकार के चित्रांकन विभिन्न अवसरों पर किये जाते हैं। मुख्यतः अंचल में बनाए जाने वाले लोक चित्र सावन में मनाए जाने वाले त्यौहार और पर्यों में बनाए जाते हैं। जिनमें प्रमुख हैं-सवनाही, नागपंचमी के चित्र, कृष्ण जन्माष्टमी के चित्र, विवाह के अवसर पर बनाये जाने वाले चित्र, चौक, कलश पर चित्रांकन, राउतों के हाथे आदि।
छत्तीसगढ़ी लोक चित्र की एक शैली 'गोदना' भी है। इसमें स्त्रियाँ अपने विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ फूल आदि चित्रित करवाती हैं। गोदना आदिवासियों के सौंदर्य और गहनों के प्रति लगाव को भी प्रदर्शित करते हैं।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक चित्रों में जहाँ एक ओर यहाँ की धार्मिक परम्पराओं और आस्थाओं का वर्णन होता है। वहीं इनमें प्रागैतिहासिक और आदिम मानव की प्रथम अनुभूतियों से उपजी परम्पराएँ भी परिलक्षित होती हैं।
नृत्य एवं संगीत कला
नृत्य कला:-
अपनी भावनाओं को शारीरिक चेष्टाओं द्वारा व्यक्त करना मानव का मूलभुत गुण है। जब तक अपनी भावनाएँ प्रदर्शित करने | के लिए उसके पास शब्दों का अभाव था, उसने सिर्फ शारीरिक चेष्टाओं से ही अपनी खुशी को प्रदर्शित किया। इस खुशी को अधिक करने के लिए उसने क्रमशः इन चेष्टाओं को लयबद्ध करना आरंभ किया।
शारीरिक लय प्रधान क्रियाओं के साथ आनन्द और सौन्दर्य की अभिव्यक्ति जिस सामूहिक रूप से होती है उसे 'लोक नृत्य' कहते हैं।
लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के निवासियों की अपनी जातीय परम्परा एवं संस्कृति का परिचायक है। छत्तीसगढ़ के अनेक लोकगीतों में से कुछ गीतों का सम्बंध नृत्य से है। करमा, डंडा और सुआ गीत नृत्य के योग से सजीव हो उठते हैं। ये नृत्य छत्तीसगढ़ के लोक-जीवन से घुल मिल गये हैं। इन नृत्यों में कुछ नृत्य पुरूषों के द्वारा तथा कुछ नृत्य स्त्रियों के द्वारा किये जाते हैं। करमा एवं डंडा पुरूष नृत्य हैं तथा सुआ स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कुछ नृत्य । स्त्री-पुरूषों दोनों के द्वारा किये जाते हैं। | जिनमें आदिवासी क्षेत्रों में किया जाने वाला नृत्य डोमकच और सरहुल प्रमुख है।
इसी तरह कुछ लोक नृत्य जाति विशिष्ट के द्वारा किये जाते हैं। इनमें राउत जाति के द्वारा किया जाने वाला गहिरा नृत्य और सतनामी लोगों के द्वारा किया जाने वाला पंथी नृत्य है।
संगीत कलाः-
जीवन और संगीत का अभिन्न सम्बंध है जिसका वास्तविक परिचय हमें लोक संगीत के माध्यम से प्राप्त होता है। लोक-संगीत में प्रेम-भक्ति, अनुराग धर्म आदि मानव जीवन के सभी अंगों का समावेश है।
छत्तीसगढ़ी अंचल में लोक संगीत में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यन्त्र- मांदर, ढोल, टिमकी, नगाड़ा, ठिसकी, तम्बूरा, चिकारा, बाँसुरी, तुरही, सिंगी आदि प्रमुख हैं।
छत्तीसगढ़ में लोक गीतों का अथाह भंडार है। वह ऐसा शाश्वत प्रवाह है जिसकी धारा में यहाँ का जनजीवन प्रवाहित होता दिखाई देता है। अपनी सम्पूर्ण सरलता के साथ -छत्तीसगढ़ का सामूहिक व्यक्तित्व यहाँ के लोक-गीतों में प्रतिबिम्बित होता है।
छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का वर्गीकरण निम्न लिखित रूप में किया जा सकता है:-
(1) संस्कार गीत:-
1. जन्म के गीत
2. विवाह के गीत
(2) पर्व गीत:-सुआ गीत, गौरा गीत, मड़ई, डंडा गीत, होली गीत, दीवाली गीत, जवारा गीत, भोजली गीत।
(3) श्रृंगार गीत:-
1. ददरिया
2. बारह मासी
(4) विविध गीत:- करमा गीत, बांस गीत, देवार गीत।
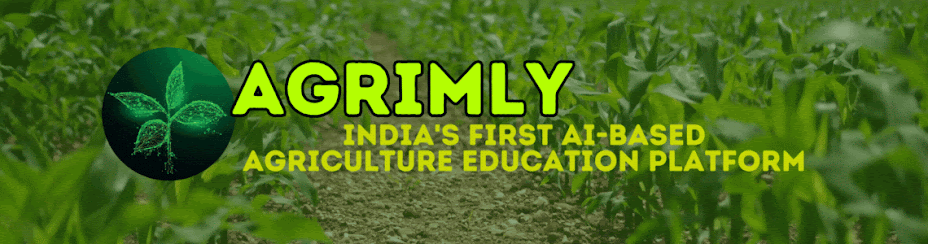
No comments:
Post a Comment
Thank You for feedback. Keep commenting on it.